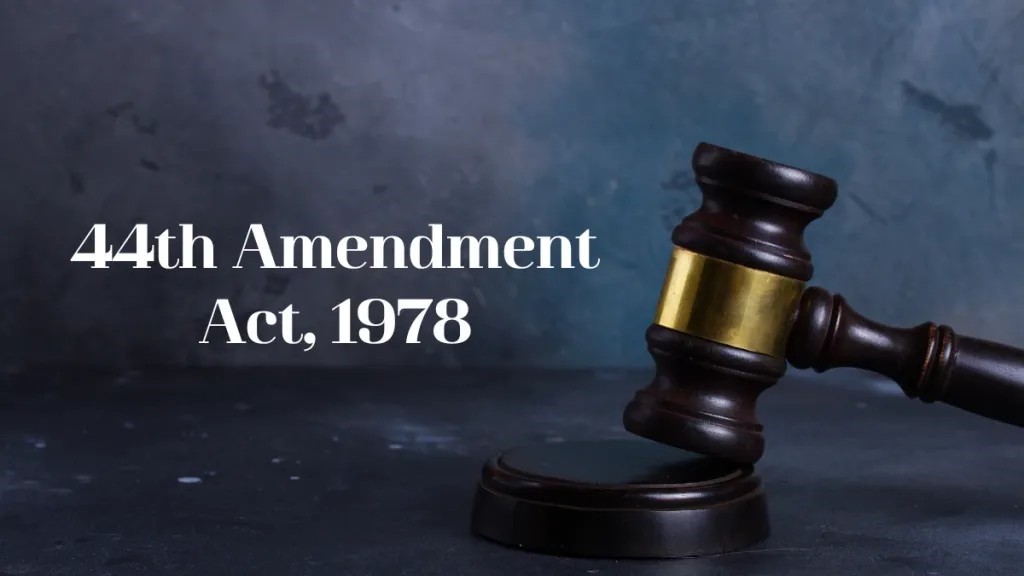
44वां संशोधन अधिनियम, 1978
44वां संशोधन अधिनियम, 1978
परिचय
जनता सरकार के कार्यकाल के दौरान पेश किए गए 44वें संवैधानिक संशोधन ने 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए कुछ बदलावों को वापस लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संशोधन ने भारतीय संविधान में व्यापक बदलाव लाए, जिससे भारत की राजनीतिक व्यवस्था की लोकतांत्रिक प्रकृति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
भारतीय संविधान में 44वां संशोधन क्या है?
1978 में लागू किए गए 44वें संशोधन अधिनियम ने 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1976 में किए गए परिवर्तनों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नागरिकों की इच्छा के विरुद्ध किए गए इन परिवर्तनों के कारण 44वें संशोधन अधिनियम को लागू करना आवश्यक हो गया। इसका उद्देश्य इन परिवर्तनों को उलटना और देश के हितों की रक्षा करना था, जिससे यह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक विकास बन गया।
44वें संशोधन अधिनियम, 1978 के उद्देश्य
- 44वां संशोधन अधिनियम, 1978 निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पेश किया गया था:
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि संसद में अस्थायी बहुमत द्वारा मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या छीना न जाए, भविष्य में ऐसी आकस्मिकता की पुनरावृत्ति के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करना आवश्यक था।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीओआई के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित करने की शक्ति का उचित रूप से और उचित विचार-विमर्श के बाद उपयोग किया जाना चाहिए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि COI के अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन की शक्ति का प्रयोग करते हुए COI की बुनियादी विशेषताओं में संसद द्वारा हल्के ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया गया था।
44वें संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधन
44वें संशोधन ने बनाया है:
मौलिक अधिकार
- संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया
- संविधान का अनुच्छेद 19(1)(एफ), जो नागरिकों को संपत्ति अर्जित करने, रखने और निपटान करने का अधिकार देता है, और संविधान का अनुच्छेद 31, जो संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित है, हटा दिया गया है
राष्ट्रपति की शक्ति
अनुच्छेद 74(1) में एक खंड शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद उन्हें दी गई किसी भी सलाह पर पुनर्विचार करे
मूल संरचना में संशोधन
संविधान की मूल संरचना में कोई भी संशोधन केवल तभी लागू किया जा सकता है जब भारत के लोग जनमत संग्रह में डाले गए बहुमत से सहमत हों, जिसमें कम से कम 51% मतदाताओं ने भाग लिया हो। अनुच्छेद 368 में संशोधन करके इसे सुनिश्चित किया जा रहा है।
संसद और राज्य विधानमंडल
अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन करके लोक सभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल पांच साल के लिए बहाल किया गया था। लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल पहले 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा 5 से 6 साल तक बढ़ाया गया था।
न्यायतंत्र
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कुछ शक्तियाँ बहाल की गईं।
इसने राष्ट्रपति, राज्यपालों और लोकसभा अध्यक्ष के चुनावों की न्यायिक समीक्षा की अनुमति दी।
राष्ट्रपति शासन
44वें संशोधन ने अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा को एक वर्ष से अधिक बढ़ाने की संसद की शक्ति पर रोक लगाने के लिए एक नया प्रावधान पेश किया।
संसदीय विशेषाधिकार
संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णयों से संबंधित अनुच्छेद 103 और 192 को यह प्रदान करने के लिए प्रतिस्थापित किया गया है कि राज्य विधानमंडल के सदस्य के मामले में, अयोग्यता के प्रश्न पर राष्ट्रपति का निर्णय निम्न पर आधारित होगा चुनाव आयोग की राय।
राष्ट्रीय आपातकाल
- इसे कार्यपालिका द्वारा आपातकालीन शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसने अनुच्छेद 352 में कई सुरक्षा उपाय पेश किए हैं। ये इस प्रकार हैं:
- 44वें संशोधन अधिनियम 1978 से पहले, युद्ध या बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की उद्घोषणा जारी की जा सकती थी। आंतरिक गड़बड़ी अस्पष्ट थी और कार्यपालिका द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा सकता था। इसलिए, अधिनियम ने आंतरिक अशांति के स्थान पर "सशस्त्र विद्रोह" अभिव्यक्ति की शुरुआत की।
- मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा के बाद ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 352 कैबिनेट को कैबिनेट रैंक के अन्य मंत्रियों के साथ प्रधान मंत्री के रूप में परिभाषित करता है। प्रारंभ में, अनुमोदन साधारण बहुमत के आधार पर होना था, लेकिन वर्तमान में इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है।
- एक बार आपातकाल की उद्घोषणा को मंजूरी मिलने के बाद कोई संसदीय नियंत्रण नहीं था। लेकिन अब अस्वीकृति पर विचार करने के लिए लोकसभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है.
- अनुच्छेद 358 के तहत, अनुच्छेद 19 स्वचालित रूप से तभी निलंबित होता है जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित किया जाता है; पहले भी इसे आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर निलंबित किया गया था.
- आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अधिनियम से पहले, आपातकाल लागू होने पर किसी या सभी मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन निलंबित किया जा सकता था।
संघवाद
अनुच्छेद 257ए, जो किसी गंभीर संकट से निपटने के लिए अपने सैन्य बलों या अन्य संघ बलों को तैनात करने की केंद्र सरकार की शक्ति से संबंधित था, हटा दिया गया।
भारतीय संविधान के 44वें संशोधन की आलोचना
- संसद को संवैधानिक संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार है। किसी विशेष निकाय के लिए संविधान में संशोधन करने का कोई प्रावधान नहीं है, जैसे कि संवैधानिक सम्मेलन (जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में) या संवैधानिक सभा।
- संविधान के एक महत्वपूर्ण हिस्से को केवल संसद द्वारा, विशेष या साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है।
- संशोधन की प्रक्रिया कानून बनाने के समान ही है।
- 44वें संशोधन अधिनियम का उद्देश्य भविष्य में संविधान की आपातकालीन धाराओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए 42वें संशोधन में विसंगतियों को सुधारना है।
- 42वें संशोधन को रद्द करने के साथ, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने संविधान की धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को बहाल करते हुए, 42वें संशोधन से पहले के अपने अधिकार क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिया।
निष्कर्ष
- 42वें संशोधन के तहत संसदीय सर्वोच्चता का फायदा उठाया जा सकता था और आपातकालीन प्रावधानों के तहत मौलिक अधिकारों को आसानी से रद्द किया जा सकता था।
- इसके परिणामस्वरूप भारत के लोगों के साथ गंभीर अन्याय हुआ और संविधान की भावना और उसमें निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ।
- परिणामस्वरूप, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, 44वां संशोधन अधिनियमित किया गया।
- भारतीय संविधान में 44वां संशोधन महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने 42वें संशोधन द्वारा संविधान में लायी गयी विकृतियों को आंशिक रूप से दूर कर दिया।