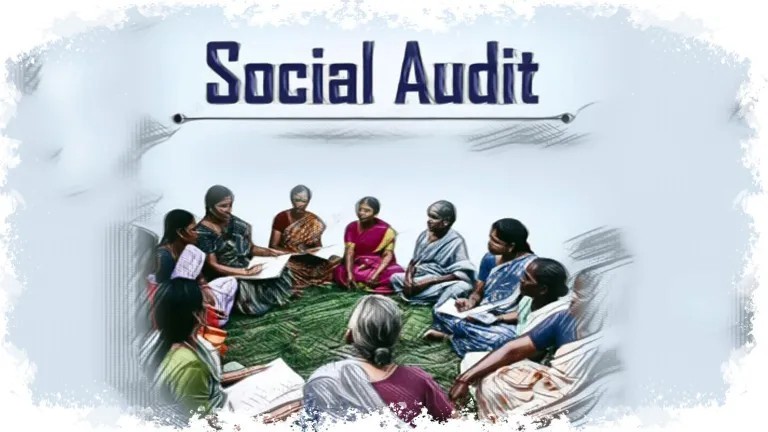
सामाजिक लेखापरीक्षा(सोशल ऑडिट)
सामाजिक लेखापरीक्षा(सोशल ऑडिट)
परिचय
सामाजिक लेखापरीक्षा का अर्थ है लोगों और सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किए गए कार्य कार्यक्रम का मूल्यांकन। यह उन कार्यक्रमों में पारदर्शिता, जवाबदेही और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक उपयोगी रणनीति है जो लोगों के लिए हैं। सामाजिक लेखापरीक्षा में इस बात की गहन जांच और विश्लेषण शामिल है कि एक सार्वजनिक इकाई अपने सामाजिक महत्व के संबंध में कैसे कार्य करती है।
सोशल ऑडिट क्या है?
- यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक संगठन या सरकार अपने हितधारकों को अपने सामाजिक प्रदर्शन का लेखा-जोखा देती है और अपने भविष्य के सामाजिक प्रदर्शन को बढ़ाने का प्रयास करती है, जिसे सामाजिक लेखापरीक्षा के रूप में जाना जाता है।
- चार्ल्स मेडावर 1972 में इस विचार को प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति थे।
- एक सामाजिक ऑडिट आपके दृष्टिकोण/लक्ष्य और वास्तविकता के साथ-साथ दक्षता और प्रभावशीलता के बीच के अंतर को कम करने में सहायता कर सकता है।
- यह हमें किसी भी सरकारी पहल या संगठन के सामाजिक प्रदर्शन का आकलन, सत्यापन, रिपोर्ट करने और बढ़ाने में सक्षम बनाता है।
- सामाजिक लेखापरीक्षा विकास लेखापरीक्षा के समान नहीं है। विकास लेखापरीक्षा और सामाजिक लेखापरीक्षा के बीच मुख्य अंतर यह है कि सामाजिक लेखापरीक्षा सामाजिक नतीजों के अक्सर नजरअंदाज किए गए विषय पर ध्यान केंद्रित करती है, जबकि विकास लेखापरीक्षा में व्यापक फोकस होता है जिसमें पर्यावरण और आर्थिक मुद्दे शामिल होते हैं, जैसे किसी परियोजना या कार्यक्रम की दक्षता।
भारत में सामाजिक लेखापरीक्षा की उत्पत्ति और विकास:
- भारत में, सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करने की पहल टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (टिस्को), जमशेदपुर द्वारा वर्ष 1979 में की गई थी।
- यह किसी संगठन की सामाजिक जवाबदेही के मापन के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित संविधान के 73वें संशोधन के बाद इसे महत्व मिला।
- 9वीं एफवाईपी (2002-07) के दृष्टिकोण पत्र में पंचायत राज संस्थानों (पीआरआई) के प्रभावी कामकाज के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा पर जोर दिया गया और ग्राम सभाओं को अपने अन्य कार्यों के अलावा एसएएस संचालित करने का अधिकार दिया गया।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 नियमित "सामाजिक लेखा परीक्षा" का प्रावधान करता है ताकि योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
ऑडिट के प्रकार:
- वित्तीय लेखापरीक्षा: वित्तीय डेटा की रिकॉर्डिंग, प्रसंस्करण, सारांश और रिपोर्टिंग की ओर निर्देशित।
- ऑपरेशनल ऑडिट: ऑपरेशन के मानक स्थापित करना, मानकों के मुकाबले प्रदर्शन को मापना, विचलन की जांच और विश्लेषण करना, सुधारात्मक कार्रवाई करना और अनुभव के आधार पर मानकों का पुनर्मूल्यांकन करना मुख्य फोकस है।
- सामाजिक लेखापरीक्षा: सामाजिक लेखापरीक्षा अपने हितधारकों के विचारों के आधार पर व्यवस्थित और नियमित निगरानी के माध्यम से किसी विभाग के गैर-वित्तीय उद्देश्यों के प्रभाव का आकलन प्रदान करता है।
सामाजिक लेखापरीक्षा के सिद्धांत
- प्रशासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता, सरकार पर यह दायित्व है कि वह सक्रिय रूप से लोगों को सभी प्रासंगिक जानकारी तक पूर्ण पहुंच प्रदान करे।
- निर्णय लेने और सत्यापन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए न केवल उनके प्रतिनिधियों बल्कि सभी प्रभावित व्यक्तियों का अधिकार आधारित अधिकार।
- ऐसे मामलों में जहां विकल्प आवश्यकता से पूर्व निर्धारित हैं, प्रभावित व्यक्तियों को एक समूह के रूप में या व्यक्तियों के रूप में, जैसा उचित हो, सूचित सहमति देने का अधिकार है
- प्रासंगिक कार्यों या निष्क्रियताओं पर सभी संबंधित और प्रभावित लोगों के प्रति निर्वाचित प्रतिनिधियों और सरकारी पदाधिकारियों की तत्काल और सार्वजनिक जवाबदेही।
सामाजिक लेखापरीक्षा का महत्व:
- यह संगठनों, विशेषकर सामाजिक और विकास गतिविधियों में लगे संगठनों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। राजस्थान सरकार ने सरकारी परियोजनाओं और कार्यक्रमों के प्रदर्शन में जवाबदेही बढ़ाने के लिए पहली बार एक सामाजिक और प्रदर्शन लेखा परीक्षा प्राधिकरण (एसपीएए) की स्थापना की है।
- राजस्थान के डूंगरपुर जिले और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के लोगों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सामूहिक रूप से सामाजिक लेखा परीक्षा का आयोजन किया है।
- इसमें विभिन्न हितधारकों की भागीदारी शामिल है और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी आवाज़ सुनने और विचार करने का अवसर प्रदान करता है।
- सामाजिक लेखापरीक्षा के माध्यम से, संगठन विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर अपने प्रभाव का आकलन और माप कर सकते हैं। यह यह निर्धारित करने में मदद करता है कि इच्छित परिणाम प्राप्त किए जा रहे हैं या नहीं और भविष्य के हस्तक्षेपों के लिए साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है।
- स्वेच्छा से सामाजिक ऑडिट करवाकर, संगठन पारदर्शिता, जवाबदेही और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं, जिससे उनके संचालन में जनता का विश्वास और भरोसा बढ़ता है।
- यह सामाजिक मुद्दों, चुनौतियों और सफलताओं के बारे में मूल्यवान डेटा और अंतर्दृष्टि उत्पन्न करता है। इस जानकारी का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण और गरीबी उन्मूलन सहित विभिन्न क्षेत्रों में नीति परिवर्तन, सुधार और सुधार की वकालत करने के लिए किया जा सकता है।
- यह संगठनों को अपनी प्रथाओं पर विचार करने, पिछले अनुभवों से सीखने और अपने प्रदर्शन में लगातार सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह आंतरिक और बाहरी हितधारकों को ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिससे प्रभावशीलता और दक्षता में वृद्धि होती है।
- यह यह सुनिश्चित करके समावेशी विकास को बढ़ावा देता है कि हाशिए पर रहने वाले और कमजोर समुदायों की जरूरतों और चिंताओं का समाधान किया जाए।
चुनौतियाँ:
- कई राज्यों में, ग्राम पंचायतों को सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों को काम पूरा होने और व्यय से संबंधित रिकॉर्ड प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है, और ग्राम सभाओं को उनकी मूल भाषाओं में सामाजिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रदान नहीं की जाती है।
- कई सरकारें सामाजिक लेखापरीक्षा इकाइयों के निदेशक के लिए आवश्यकताओं में निर्दिष्ट पारदर्शी चयन प्रक्रिया का पालन नहीं करती हैं। कई सामाजिक लेखापरीक्षा इकाइयों के पास वर्ष में एक बार भी सभी पंचायतों को कवर करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं।
- ऑडिटर कार्यान्वयन एजेंसियों के अधीन होते हैं जिन्हें प्रतिरोध और धमकी का सामना करना पड़ता है और सत्यापन के लिए मूल डेटा तक पहुंच पाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि सरकार ने सोशल ऑडिट के संस्थागतकरण को विनियमित नहीं किया है।
- व्यक्तियों के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए बहुत कम या कोई प्रोत्साहन नहीं।
- मानकीकरण का अभाव - वित्तीय रिपोर्टिंग के विपरीत, सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए कोई सार्वभौमिक मानक नहीं है।
- जागरूकता और शिक्षा की कमी - कुछ संगठन और हितधारक सामाजिक ऑडिट की अवधारणा और उनके लाभों को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। जागरूकता की यह कमी ऑडिट के सफल कार्यान्वयन में बाधा बन सकती है।
भारत में सामाजिक लेखापरीक्षा:
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 नियमित "सामाजिक लेखा परीक्षा" का प्रावधान करता है ताकि योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
- मेघालय भारत का पहला राज्य था जिसने मेघालय सामुदायिक भागीदारी और लोक सेवा सामाजिक लेखापरीक्षा अधिनियम, 2017 को लागू किया। इस प्रकार, उन्होंने कानून द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा को अनिवार्य बना दिया।
- आंध्र प्रदेश - आंध्र प्रदेश में, सोसाइटी फॉर सोशल ऑडिट, एकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी की स्थापना सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त एक स्वतंत्र संगठन के रूप में की गई थी। एसए को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश राज्य अन्य सभी राज्यों के लिए एक मॉडल बनकर उभरा है।
आगे बढ़ने का रास्ता:
- राजनीतिक प्रशासन और कार्यान्वयन एजेंसियों को जवाबदेह बनाए रखने के लिए नागरिक समूहों की स्थापना महत्वपूर्ण है। इन समूहों को सामाजिक अंकेक्षण को बढ़ाने की वकालत करनी चाहिए।
- सामाजिक अंकेक्षण समिति के सदस्यों के मार्गदर्शन हेतु सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञों की एक टीम गठित की जाय।
- सामाजिक लेखापरीक्षा प्रथाओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास, जैसे रिपोर्ट आयोजित करना और लिखना और ग्राम सभा में प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- विश्वविद्यालय के छात्रों सहित व्यक्तियों को ग्राम संसाधन व्यक्तियों के रूप में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। उदाहरण के लिए, झारखंड ने सामाजिक लेखा परीक्षा पैनल में शामिल होने के लिए नागरिक समाज के प्रमुख सदस्यों को आमंत्रित करके एक औपचारिक प्रणाली स्थापित की है।
- सामाजिक लेखापरीक्षा प्रणाली को एक संस्थागत संरचना बनाने के लिए जिसे निहित स्वार्थों द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती, इसके लिए विभिन्न अधिकारियों से व्यापक समर्थन और प्रोत्साहन की आवश्यकता है।
- ऐसे नियम स्थापित किए जाने चाहिए जो कार्यान्वयन एजेंसियों को सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया में भाग लेने और निष्कर्षों पर तेजी से कार्य करने के लिए बाध्य करें।
- राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट नियम स्थापित करने चाहिए कि सामाजिक लेखापरीक्षा परिणाम कानूनी रूप से स्वीकृत हों।
- एमआईएस का उपयोग सभी स्तरों पर योजनाओं की बारीकियों पर नज़र रखकर कार्यक्रम के जीवन चक्र की योजना, कार्यान्वयन और फीडबैक चरणों को सुव्यवस्थित कर सकता है।
- राज्य सरकार को जिम्मेदार पक्षों की पहचान करने और दोषपूर्ण एसएयू कर्मचारियों के साथ-साथ अन्य जमीनी स्तर के लेखा परीक्षकों को दंडित करने के लिए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय को सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर कार्यान्वयन एजेंसी की प्रतिक्रिया का निरीक्षण करना चाहिए। कार्रवाई रिपोर्ट की निगरानी के लिए एसएयू, कार्यान्वयन एजेंसियों और एमओआरडी अधिकारियों के बीच एक त्रैमासिक बैठक बुलाई जानी चाहिए।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत को हर छह महीने में एक बार इसका संचालन करना चाहिए।
- मीडिया का लक्ष्य ग्रामीण समुदायों तक पहुंचना और विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना होना चाहिए जो ग्रामीण चिंता के मामलों, विशेष रूप से ग्राम सभाओं और सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए उनकी क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हैं।