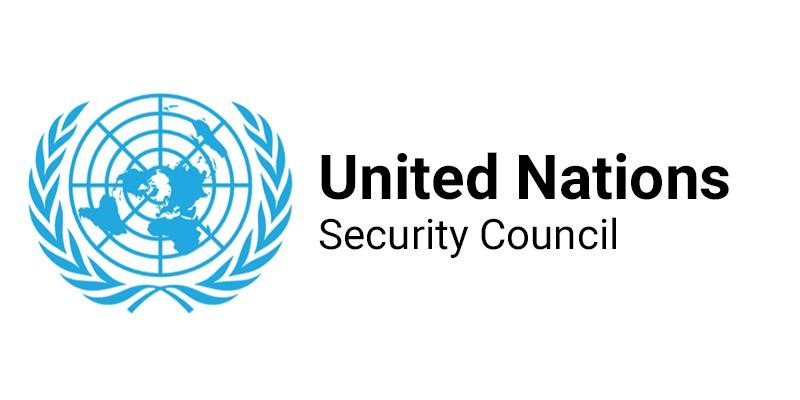
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी)
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी)
परिचय
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की स्थापना 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक अंतरराष्ट्रीय निकाय के रूप में की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य संघर्षों को रोकना और हल करना, शांति मिशनों को अधिकृत करना और वैश्विक स्थिरता के लिए खतरों का जवाब देना है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के भीतर एक प्राथमिक निकाय है जो वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। वीटो शक्ति वाले पांच स्थायी सदस्यों (चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका) सहित 15 सदस्य राज्यों से युक्त, यूएनएससी सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों के लिए बाध्यकारी निर्णय ले सकता है।
संरचना
यूएनएससी को अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए संरचित किया गया है।
सदस्यता:
यूएनएससी 15 सदस्य देशों से बना है, जिसमें पांच स्थायी सदस्य (चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका) और दस गैर-स्थायी सदस्य दो साल के कार्यकाल के लिए महासभा द्वारा चुने जाते हैं।
स्थायी सदस्य और वीटो शक्ति:
पाँच स्थायी सदस्यों, जिन्हें अक्सर P5 कहा जाता है, के पास वीटो शक्ति होती है, जो उन्हें किसी भी ठोस प्रस्ताव को अवरुद्ध करने की अनुमति देती है। यह अनूठी विशेषता यूएनएससी निर्णयों में इन राज्यों को महत्वपूर्ण प्रभाव देती है।
अध्यक्षता:
यूएनएससी की अध्यक्षता अपने सदस्य राज्यों के बीच मासिक रूप से बदलती रहती है। राष्ट्रपति बैठकों की अध्यक्षता करता है, एजेंडा तय करता है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर परिषद का प्रतिनिधित्व करता है।
समितियाँ:
UNSC में विभिन्न समितियाँ और कार्य समूह हैं, जैसे प्रतिबंध समितियाँ, जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रतिबंधों और शांति मिशनों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों से निपटती हैं।
अधिदेश एवं उत्तरदायित्व
यूएनएससी का अधिदेश संयुक्त राष्ट्र अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से परिभाषित है और इसमें कई प्रमुख जिम्मेदारियां शामिल हैं।
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का रखरखाव:
यूएनएससी का प्राथमिक उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरों की पहचान करना और संघर्षों को रोकने, संकटों का जवाब देने और आवश्यक होने पर सैन्य कार्रवाई को अधिकृत करने के लिए उचित उपाय करना है।
संघर्ष समाधान और शांति स्थापना:
यूएनएससी युद्धविराम, बातचीत और स्थिरता की ओर परिवर्तन की सुविधा के लिए संघर्ष क्षेत्रों में शांति मिशन और विशेष राजनीतिक मिशन स्थापित कर सकता है।
प्रतिबंध:
यूएनएससी के पास राज्यों और संस्थाओं पर अपने निर्णयों और अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने के लिए दबाव डालने के लिए हथियार प्रतिबंध और आर्थिक उपायों सहित प्रतिबंध लगाने का अधिकार है।
संकल्पों को अपनाना:
यूएनएससी शांति समझौतों, अंतर्राष्ट्रीय कानून और शांति मिशनों की स्थापना सहित सुरक्षा मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर प्रस्तावों को अपनाता है।
मानवाधिकारों का संरक्षण:
यूएनएससी उन स्थितियों का समाधान कर सकता है जहां मानवाधिकारों का हनन अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है, कमजोर आबादी की रक्षा के लिए कार्रवाई को अधिकृत कर सकता है।
अप्रसार और निरस्त्रीकरण:
यूएनएससी परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों के अप्रसार और राज्यों और गैर-राज्य अभिनेताओं के निरस्त्रीकरण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है।
यूएनएससी की चुनौतियां
- प्रतिनिधित्व और सुधार: एक सतत चिंता प्रतिनिधित्व और यूएनएससी के भीतर सुधार की आवश्यकता के इर्द-गिर्द घूमती है। कई लोग वर्तमान संरचना को, विशेष रूप से पी5 सदस्यों के पास मौजूद वीटो शक्ति को पुराना और अप्रमाणिक मानते हैं।
- वीटो शक्ति: आलोचकों का तर्क है कि वीटो शक्ति का दुरुपयोग या निर्णय लेने में रुकावट हो सकती है, क्योंकि कोई भी P5 सदस्य प्रस्तावों को अवरुद्ध कर सकता है, भले ही अन्य सदस्य राज्यों द्वारा व्यापक रूप से समर्थित हो।
- क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व: कुछ क्षेत्र, विशेष रूप से अफ्रीका, कम प्रतिनिधित्व महसूस करते हैं और अपने प्रभाव और अद्वितीय चुनौतियों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए स्थायी सीटों सहित बढ़े हुए प्रतिनिधित्व की वकालत करते हैं।
- निर्णय लेने की प्रक्रिया: एजेंडा तय करने और प्रस्तावों को आकार देने में पी5 सदस्यों का प्रभुत्व निर्णय लेने की प्रक्रिया में समावेशिता और पारदर्शिता के बारे में चिंताएं पैदा करता है।
- वैश्विक संकटों पर प्रतिक्रिया: संघर्षों और मानवीय आपात स्थितियों जैसे वैश्विक संकटों पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने की यूएनएससी की क्षमता पर बहस हुई है। कुछ लोगों का तर्क है कि परिषद की निर्णय लेने की क्षमता और वीटो शक्ति त्वरित और निर्णायक कार्रवाई में बाधा डालती है।
- प्रवर्तन और कार्यान्वयन: कुछ मामलों में, सदस्य राज्यों ने प्रस्तावों का पूरी तरह से अनुपालन नहीं किया है, जिससे परिषद की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता कम हो गई है।
संयुक्त राष्ट्र के वित्तपोषण में मुद्दे
- शांतिरक्षा बजट असमानता: लगभग 40 संयुक्त राष्ट्र मिशनों और शांति-रक्षा अभियानों में 95,000 सैनिकों, पुलिस और नागरिक कर्मियों को शामिल करने के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा बजट केवल 6 अरब डॉलर से अधिक है। शांति मिशनों से संबंधित निर्णयों पर अक्सर UNSC P5 सदस्यों का वर्चस्व होता है, भले ही कई सैनिक अन्य देशों से आते हैं।
- अवैतनिक मूल्यांकन: सदस्य राष्ट्रों पर आम बजट में मूल्यांकन योगदान का बकाया $711 मिलियन है।
- स्वैच्छिक योगदान पर निर्भरता: मानवीय सहायता, विकासात्मक कार्य और विशेष एजेंसियां स्वैच्छिक योगदान पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं, जिससे फंडिंग कम पूर्वानुमानित हो जाती है और संभावित रूप से दानदाताओं की प्राथमिकताओं के प्रति पक्षपाती हो जाती है।
- जलवायु परिवर्तन वित्तपोषण: विकसित देशों ने विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त में 100 बिलियन डॉलर प्रदान करने के अपने वादे को पूरा नहीं किया है, बावजूद इसके कि उनका ऐतिहासिक उत्सर्जन वर्तमान जलवायु परिवर्तन का प्राथमिक कारण है, जो विकासशील देशों को असमान रूप से प्रभावित कर रहा है।
भारत और यूएनएससी
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में अपनी भूमिका और प्रतिनिधित्व को लेकर भारत की लगातार चिंताएं और लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे हैं। इन चिंताओं में कई प्रमुख पहलू शामिल हैं:
1. स्थायी सदस्यता की अनुपस्थिति: भारत का दावा है कि स्थायी सदस्य के रूप में इसकी अनुपस्थिति वर्तमान वैश्विक भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करने में विफल रहती है और राष्ट्रों के बीच अधिक न्यायसंगत प्रतिनिधित्व की खोज में बाधा उत्पन्न करती है।
2. निर्णय लेने में सीमित प्रभाव: पांच मौजूदा स्थायी सदस्यों के पास पर्याप्त प्रभाव और निर्णय लेने का अधिकार है, जबकि गैर-स्थायी सदस्यों को परिषद के एजेंडे और प्रस्तावों को आकार देने के लिए कम अवसर दिए जाते हैं।
3. महत्वपूर्ण मामलों पर आवाज पर प्रतिबंध: भारत का मानना है कि उसके दृष्टिकोण और योगदान, विशेष रूप से शांति स्थापना, आतंकवाद विरोधी और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में, यूएनएससी चर्चाओं और निर्णयों में पर्याप्त मान्यता नहीं मिलती है।
4. आतंकवाद विरोधी प्रयास: भारत, आतंकवाद के कृत्यों का अनुभव करते हुए, आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और उपायों को बढ़ाने की वकालत करता है। आतंकवाद को परिभाषित करने और पड़ोसी देशों से उत्पन्न सीमा पार आतंकवाद को संबोधित करने पर वैश्विक सहमति बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार की आवश्यकता
- भारत ने अपनी समावेशिता और लोकतांत्रिक प्रकृति को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सुधार के लिए सक्रिय रूप से वकालत की है।
- भारत परिषद की सदस्यता के विस्तार की वकालत करता है, जिसमें अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों को स्थायी सीटें देना शामिल होगा।
- इस प्रस्तावित सुधार का उद्देश्य यूएनएससी को समकालीन वैश्विक परिदृश्य के साथ बेहतर ढंग से जोड़ना है।
- भारत एक ऐसी निर्णय लेने की प्रक्रिया के महत्व को रेखांकित करता है जो अधिक व्यापक और जवाबदेह हो, जो सभी सदस्य राज्यों की चिंताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखे।
- यूएनएससी में सुधार के लिए भारत की प्रतिबद्धता और बहुपक्षवाद के प्रति उसकी प्रतिबद्धता वैश्विक शासन को इस तरह से आकार देने के उसके चल रहे प्रयासों को दर्शाती है जिससे विकासशील देशों के हितों को लाभ हो।
आगे बढ़ने का रास्ता
- राजनयिक पहलों को सुदृढ़ करें: भारत को अपने राजनयिक प्रयासों को जारी रखना चाहिए, विशेष रूप से स्थायी सदस्यता सुरक्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के स्थायी सदस्यों के साथ जुड़ने में।
- योगदान और नेतृत्व को उन्नत करें: भारत को वैश्विक शांति, सुरक्षा और प्रगति के प्रति अपने अटूट समर्पण को प्रदर्शित करते हुए संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों, आतंकवाद विरोधी प्रयासों और सतत विकास परियोजनाओं में अपनी सक्रिय भागीदारी जारी रखनी चाहिए।
- चैंपियन समावेशिता और पारदर्शिता: इसमें गैर-स्थायी सदस्यों को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि सभी सदस्य राज्यों को संकल्पों को आकार देने में समान अवसर मिले।
- क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करें: भारत हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के भीतर अपनी पहल बढ़ा सकता है।
- नागरिक समाज और गैर-सरकारी संस्थाओं के साथ जुड़ना: सार्वजनिक समर्थन बनाना और एक व्यापक गठबंधन जुटाना भारत के प्रभाव को बढ़ा सकता है और सार्थक सुधारों के लिए दबाव बढ़ा सकता है।
- बहुपक्षीय उपक्रमों में भाग लें: भारत को ब्रिक्स, जी20 और आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठनों में अपनी सक्रिय भूमिका बनाए रखनी चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) का क्या महत्व है? UNSC में सुधारों की आवश्यकता पर चर्चा करें।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
1.यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र अंग है जिसके पास निर्णय लेने की शक्ति है जिसे सदस्य देश लागू करने के लिए बाध्य हैं।
2.हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा दो साल के कार्यकाल के लिए कुल 10 में से यूएनएससी के लिए पांच गैर-स्थायी सदस्यों का चुनाव करती है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2
उत्तर C