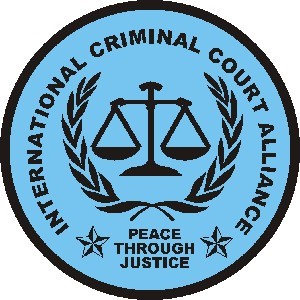
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी)
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी)
परिचय
- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) दुनिया का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, जो रोम संविधि के नाम से जानी जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा शासित होता है।
- न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है।
- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) जांच करता है और, यदि आवश्यक हो, तो नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रामकता जैसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता के सबसे गंभीर अपराधों के आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है।
- रोम संविधि में कहा गया है कि जब भी न्यायाधीश आवश्यक समझें तो न्यायालय कहीं और बैठक आयोजित कर सकता है।
- न्यायालय दंडमुक्ति को समाप्त करने के लिए एक वैश्विक लड़ाई में भाग ले रहा है, और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय के माध्यम से, यह उम्मीद करता है कि जिम्मेदार लोगों को उनके अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा और भविष्य में इसी तरह के अपराधों को होने से रोकने में मदद मिलेगी।
- न्यायालय इन उद्देश्यों को अकेले हासिल नहीं कर सकता। यह राष्ट्रीय अदालतों को अंतिम उपाय की अदालत के रूप में प्रतिस्थापित करने के बजाय पूरक बनाने का प्रयास करता है।
- भारत ने राष्ट्रीय हितों, राज्य संप्रभुता, निष्पक्ष अभियोजकों को प्राप्त करने में कठिनाइयों, साक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई और अपराध को परिभाषित करने में कठिनाई के कारण रोम संविधि का अनुमोदन नहीं करने का निर्णय लिया।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय - ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- बीसवीं सदी के संघर्षों के दौरान, कुछ सबसे जघन्य अपराध किये गये। दुर्भाग्य से, इनमें से कई अंतरराष्ट्रीय कानून उल्लंघनों को दंडित नहीं किया गया है।
- जब 1948 में नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर कन्वेंशन को अपनाया गया, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में हुए अत्याचारों के प्रकारों से निपटने के लिए एक स्थायी अंतरराष्ट्रीय अदालत की आवश्यकता को पहचाना।
- शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय प्रणाली की अवधारणा फिर से उभरी।
- हालाँकि, जब संयुक्त राष्ट्र आईसीसी क़ानून पर बहस कर रहा था, दुनिया ने पूर्व यूगोस्लाविया और रवांडा के क्षेत्र में जघन्य अपराधों को होते देखा।
- इन अत्याचारों के जवाब में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इनमें से प्रत्येक मामले में तदर्थ न्यायाधिकरण की स्थापना की।
- इन घटनाओं का उस सम्मेलन को आयोजित करने के निर्णय पर निर्विवाद प्रभाव पड़ा जिसने 1998 की गर्मियों में रोम में आईसीसी की स्थापना की।
- 160 राज्यों के एक सम्मेलन ने 17 जुलाई 1998 को पहली संधि-आधारित स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत की स्थापना की।
- उस सम्मेलन में अपनाई गई संधि को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम संविधि के रूप में जाना जाता है।
- यह अन्य बातों के अलावा, आईसीसी के अधिकार क्षेत्र के तहत होने वाले अपराधों, प्रक्रिया के नियमों और राज्यों के लिए आईसीसी के साथ सहयोग करने के तंत्र को स्थापित करता है।
संरचना
आईसीसी की संरचना इसके उचित कामकाज और अंतर्राष्ट्रीय न्याय के अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थित की गई है।
- राज्यों की पार्टियों की सभा (एएसपी): एएसपी उन सदस्य राज्यों से बनी है जिन्होंने रोम संविधि की पुष्टि की है। यह आईसीसी के निरीक्षण और विधायी निकाय के रूप में कार्य करता है, जो बजटीय और नीतिगत निर्णय लेता है।
- प्रेसीडेंसी: प्रेसीडेंसी में आईसीसी का प्रतिनिधित्व करने वाले उनके साथियों द्वारा चुने गए तीन न्यायाधीश होते हैं। राष्ट्रपति न्यायालय के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- अभियोजक का कार्यालय: अभियोजक आईसीसी के अधिकार क्षेत्र के भीतर अपराधों के लिए जांच शुरू करने और व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए जिम्मेदार है।
- रजिस्ट्रार का कार्यालय: रजिस्ट्रार अदालत के प्रशासन के गैर-न्यायिक पहलुओं के लिए जिम्मेदार है, जिसमें पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा, अदालत प्रबंधन और न्यायाधीशों और कानूनी कर्मचारियों के लिए समर्थन शामिल है।
- चैंबर: आईसीसी में न्यायाधीशों के तीन विभाग हैं जो मामलों की सुनवाई करते हैं: प्री-ट्रायल चैंबर, ट्रायल चैंबर और अपील चैंबर। वे अभियुक्त के अपराध या निर्दोषता का निर्धारण करने और सजा सुनाने के लिए जिम्मेदार हैं।
अधिदेश एवं क्षेत्राधिकार
आईसीसी के पास सबसे गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों की जांच करने और मुकदमा चलाने का स्पष्ट और व्यापक अधिदेश है।
मानवता के विरुद्ध अपराध: आईसीसी नागरिक आबादी पर व्यापक और व्यवस्थित हमलों को संबोधित करता है, जिसमें हत्या, दासता, यौन हिंसा और अन्य अमानवीय कृत्य शामिल हैं।
नरसंहार: किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूर्ण या आंशिक रूप से नष्ट करने के इरादे से किए गए कृत्यों पर आईसीसी का अधिकार क्षेत्र है।
युद्ध अपराध: आईसीसी युद्ध के कानूनों और रीति-रिवाजों के उल्लंघन पर मुकदमा चलाता है, जैसे कि नागरिकों को निशाना बनाना, प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल करना और युद्धबंदियों के साथ दुर्व्यवहार करना।
आक्रामकता: आक्रामकता के अपराध पर आईसीसी का अधिकार क्षेत्र 2018 में सक्रिय किया गया था, जिससे दूसरे राज्य के खिलाफ आक्रामकता के कृत्यों की योजना बनाने, शुरू करने या निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई।
आलोचना
- आईसीसी की आम तौर पर पक्षपात के लिए आलोचना की जाती है, छोटे और शक्तिहीन राज्यों के कमांडरों को दंडित करने जबकि अमीर और मजबूत राज्यों द्वारा किए गए अपराधों से बचने के लिए इसकी आलोचना की जाती है।
- 2016 तक आईसीसी जिन 9 मामलों पर काम कर रही थी वो सभी अफ़्रीकी देशों के थे. अमेरिकी विदेश विभाग का दावा है कि आईसीसी के न्यायाधीशों और अभियोजकों के अधिकार पर अपर्याप्त जाँच और संतुलन है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून के उल्लंघन की जांच और अभियोजन के अनुरोध और पर्यवेक्षण के भार को हटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना की गई थी।
- आमतौर पर आईसीसी को अप्रभावी, अक्षम और महंगा होने के लिए दोषी ठहराया जाता है, क्योंकि पंद्रह वर्षों की अवधि में केवल चार दोषसिद्धि (कटंगा, थॉमस लुबंगा, जेन पियरे बेम्बा और अल महदी) पर निर्णय दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिन पर कभी-कभी ध्यान नहीं दिया जाता है। किसी व्यक्ति के खिलाफ मामला तैयार करने से पहले अभियोजक के कार्यालय को देश में स्थिति की जांच करनी चाहिए ताकि यह जांचा जा सके कि क्या अदालत आरोपियों को निर्धारित करने और उनके खिलाफ मामला बनाने के लिए कार्रवाई कर सकती है।
- नरसंहार के मामले, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध बहुत जटिल हैं और इसमें विदेशी प्राधिकरण से बड़ी मात्रा में सबूतों से निपटना शामिल है। जैसा कि यह ध्यान देने योग्य है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का विरोध करने वाले तदर्थ पैनल केवल पहले स्थान पर ही चौकस हैं। पिछले यूगोस्लाविया के लिए अंतर्राष्ट्रीय पैनल और रवांडा के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पैनल, इस प्रकार के मामलों में समय और संसाधन लगते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय कानून और न्याय में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतिनिधित्व करता है। गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों के लिए व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराने का इसका जनादेश दण्डमुक्ति को समाप्त करने, जवाबदेही को बढ़ावा देने और भविष्य में होने वाले अत्याचारों को रोकने में योगदान देता है। चुनौतियों और आलोचना का सामना करते हुए, आईसीसी अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सबसे जघन्य अपराधों के लिए न्याय और जवाबदेही हासिल करने के वैश्विक प्रयास में एक आवश्यक संस्था बनी हुई है।
|
कानूनी प्रक्रिया से सम्बंधित अन्य तथ्य
|
भारत और आईसीसी
भारत ने रोम क़ानून का अनुमोदन नहीं किया है और परिणामस्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) का सदस्य नहीं है। भारत के ICC से दूर रहने के कारण इस प्रकार हैं:
- शक्तिशाली राज्यों के संभावित प्रभाव के कारण निष्पक्ष अभियोजकों को सुरक्षित रखने में चुनौतियाँ।
- कमजोर राज्य संप्रभुता के बारे में चिंताएं, क्योंकि उस देश में व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने की मांग हो सकती है जहां अपराध हुआ है।
- जटिल क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दों और कई हितधारकों और राज्यों की भागीदारी को देखते हुए साक्ष्य एकत्र करने में कठिनाइयाँ।
- अपराधों की आईसीसी की परिभाषा पर असहमति, विशेष रूप से सीमा पार आतंकवाद और परमाणु हथियारों के उपयोग से जुड़े मामलों में।
- राष्ट्रीय हित का विचार, क्योंकि भारत का मानना है कि आईसीसी अपने मामलों में चयनात्मक है, जो सार्वभौमिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है।
- आईसीसी अभियोजक में निहित पर्याप्त शक्ति की आलोचना, जो राज्य के रेफरल या न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर व्यक्तियों और संगठनों से जानकारी के आधार पर जांच शुरू कर सकता है।
आगे बढ़ने का रास्ता
- आईसीसी को अपनी वैधता बढ़ाने के लिए राजनीतिक दिखावे के बजाय निष्पक्षता को प्राथमिकता देनी चाहिए। सदस्य देशों को गवाही देने के इच्छुक अपराध पीड़ितों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाना चाहिए और उन्हें आगे की धमकियों और हिंसा से बचाना चाहिए।
- आईसीसी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्याय संघर्ष के बाद के समाजों में दीर्घकालिक शांति, स्थिरता और न्यायसंगत विकास में योगदान दे सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
i) अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय एक अंतरसरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है जो हेग, नीदरलैंड में बैठता है
ii) अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की रोम संविधि वह संधि है जिसने चार प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की स्थापना की: नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता का अपराध।
iii) भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) पर रोम क़ानून पर हस्ताक्षर किए हैं लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है।
उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?
ए) केवल 1
बी) केवल 1 और 2
C) केवल 2 और 3
D) 1, 2 और 3
उत्तर डी
भारत उन देशों में से है जिसने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम क़ानून पर न तो हस्ताक्षर किए हैं और न ही इसे स्वीकार किया है। भारत सरकार द्वारा रोम संविधि को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं? चर्चा करना।