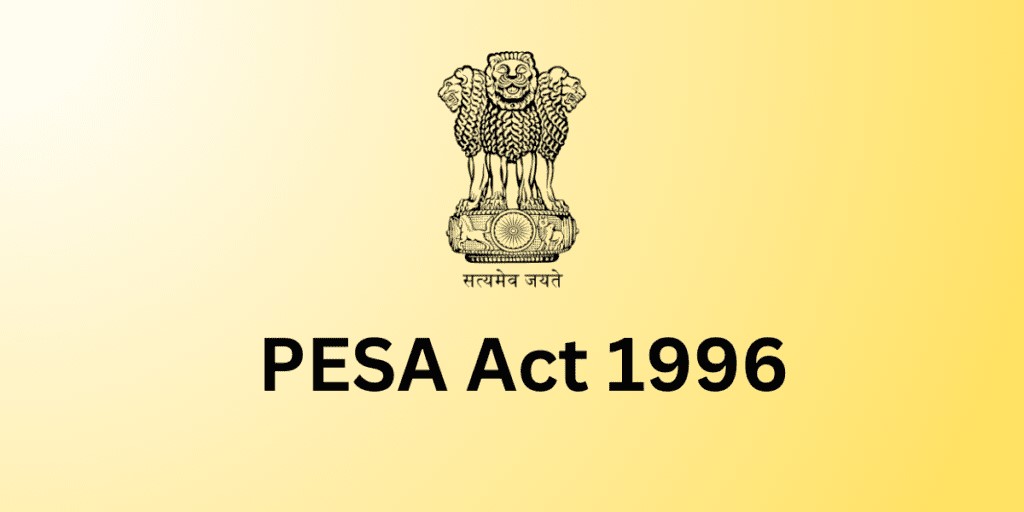
पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा)
पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा)
पेसा अधिनियम 1996 - ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- पंचायती राज (भाग IX) संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में शामिल है और राज्यों को ही पंचायतों को शक्तियों के हस्तांतरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- जबकि पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों को संविधान के भाग IX से छूट दी गई है, संविधान के अनुच्छेद 243M में कहा गया है कि संसद अपने प्रावधानों को कानून द्वारा अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों तक बढ़ा सकती है, ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन जो ऐसे कानून में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं और कोई नहीं ऐसे कानून को संविधान में संशोधन माना जाएगा।
- इसे 1996 में भूरिया समिति की रिपोर्ट के जवाब में अधिनियमित किया गया था, जिसने सिफारिश की थी कि संविधान के भाग IX को विशिष्ट समायोजन और अपवादों के साथ अनुसूचित V क्षेत्रों तक बढ़ाया जाए।
- आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना उन दस राज्यों में से हैं जिनमें अनुसूचित V क्षेत्र हैं।
- राज्यों में पेसा के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज मंत्रालय नोडल मंत्रालय है।
पेसा कानून क्या है?
- इसे 1996 में "पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग IX के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए" अधिनियमित किया गया था।
- भाग IX, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 243-243ZT शामिल हैं, में नगर पालिकाओं और सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
पेसा अधिनियम के प्रावधान
- PESA अधिनियम को पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य भारत में अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाना है।
- आदिवासी क्षेत्रों में निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में ग्राम सभाओं को मान्यता।
- भूमि, जल और वन जैसे प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए ग्राम सभाओं को अधिकार देना।
- भूमि अधिग्रहण और विकास परियोजनाओं के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया में आदिवासी समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- जनजातीय समुदायों के पारंपरिक अधिकारों और रीति-रिवाजों की रक्षा करना।
- अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को स्वायत्तता प्रदान करना। यह सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए किया जाता है।
- अनुसूचित क्षेत्रों में सरकार के उच्च स्तर से पंचायतों को कुछ शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना।
- आदिवासी संस्कृति, विरासत और परंपराओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- जनजातीय समुदायों के बीच स्वशासन और आत्मनिर्णय को बढ़ावा देना।
- अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों की प्रशासनिक और वित्तीय क्षमताओं को मजबूत करना।
- स्थानीय स्तर पर संघर्ष समाधान और विवाद निपटान के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करना।
- अधिनियम के तहत, अनुसूचित क्षेत्र वे हैं जो अनुच्छेद 244(1) में संदर्भित हैं, जो कहता है कि पांचवीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू होंगे।
- पांचवीं अनुसूची इन क्षेत्रों के लिए कई विशेष प्रावधानों का प्रावधान करती है।
PESA लागू करने का उद्देश्य:
- पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग IX के प्रावधानों को कुछ संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करना।
- जनजातीय आबादी के बड़े हिस्से को स्व-शासन प्रदान करना।
- सहभागी लोकतंत्र के साथ ग्राम प्रशासन स्थापित करना और ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र बनाना।
- पारंपरिक प्रथाओं के अनुरूप एक उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा विकसित करना।
- जनजातीय समुदायों की परंपराओं और रीति-रिवाजों की सुरक्षा और संरक्षण करना।
पेसा अधिनियम, 1996 की मुख्य विशेषताएं
- अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए बनाया गया राज्य कानून स्थानीय समुदायों की पारंपरिक परंपराओं और कानूनों के अनुरूप होना चाहिए।
- एक गाँव में बस्तियाँ, बस्तियाँ या बस्तियों और बस्तियों का समूह शामिल होगा, जबकि इसमें एक समुदाय शामिल होगा जो समुदाय की परंपराओं और कानूनों के अनुसार अपने मामलों का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार है।
- प्रत्येक गाँव में एक ग्राम सभा होनी चाहिए जिसमें गाँव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी मतदाता शामिल होंगे।
- ग्राम सभा गांव के लोगों के रीति-रिवाजों और परंपराओं की रक्षा के लिए जिम्मेदार होगी।
- ग्राम स्तर पर कार्यान्वयन के लिए उठाए जाने से पहले ग्राम सभा को विकास की योजनाओं के अनुमोदन के लिए भी जिम्मेदार होना चाहिए।
- ग्राम सभा विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए पात्र लोगों की पहचान करने के लिए जिम्मेदार होगी।
- इन कार्यक्रमों के लिए धन का उपयोग करने के लिए ग्राम स्तर पर पंचायत को ग्राम सभा से प्रमाणीकरण प्राप्त करना चाहिए।
- पंचायत में एससी और एसटी समुदायों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाएंगी। एसटी के लिए आरक्षण कुल सीटों का कम से कम आधा होना चाहिए और पंचायतों के सभी स्तरों पर अध्यक्षों की सीटें केवल एसटी समुदाय के लिए आरक्षित होंगी।
- यदि समुदाय को पंचायत में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो मध्यवर्ती और जिला स्तर की पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों से व्यक्तियों को नामांकित किया जा सकता है। यह नामांकन राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा. नामांकित किये जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या पंचायत के कुल सदस्यों के दसवें हिस्से से अधिक नहीं हो सकती।
- राज्य सरकार को अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण से पहले और इन क्षेत्रों में लोगों के पुनर्वास से पहले ग्राम सभा से परामर्श करने की आवश्यकता है लेकिन परियोजनाओं का वास्तविक कार्यान्वयन राज्य सरकार के हाथों में होगा।
- अनुसूचित क्षेत्रों में जल निकायों के रखरखाव के लिए उचित स्तर पर पंचायत जिम्मेदार होगी।
- अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिजों के खनन के लिए लाइसेंस देने के लिए उचित स्तर पर ग्राम सभा या पंचायत से अनुशंसा प्राप्त करना अनिवार्य है।
- राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों को निम्नलिखित से संबंधित शक्तियाँ दी जाएँ:
- नशीले पदार्थों के उपयोग या बिक्री पर रोक लगाएं
- बांस जैसी लघु वन उपज का स्वामित्व
- इन क्षेत्रों में लोगों के अलगाव को रोकें और यदि अलगाव पहले ही हो चुका है तो लोगों का पुनर्वास करें
- ग्रामीण बाजारों से संबंधित मामलों का प्रबंधन करना
- इन क्षेत्रों में धन उधार पर नियंत्रण रखें
- स्थानीय सामाजिक संस्थाओं पर नियंत्रण रखें
- राज्य विधायिका को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऊपरी स्तर की पंचायतें निचले स्तर की पंचायतों या ग्राम सभा की शक्तियों को ग्रहण न करें
- कोई भी कानून जो लागू है लेकिन इस अधिनियम से असंगत है, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद लागू नहीं रहेगा। इस अधिनियम से पहले जो पंचायतें सत्ता में हैं वे अपने कार्यकाल तक बनी रहेंगी लेकिन राज्य विधानमंडल द्वारा उन्हें जल्द ही भंग किया जा सकता है।
अधिनियम को लागू करने का महत्व
- लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण: PESA ग्राम सभाओं को सभी सामाजिक क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण अधिकार और विकास योजनाओं को मंजूरी देने की क्षमता देता है। इसमें निम्नलिखित पर नियंत्रण शामिल है:
- जल, जंगल, जमीन (जल, जंगल और जमीन) पर संसाधन
- लघु वनोपज
- मानव संसाधन: प्रक्रियाएं और कार्मिक जो नीतियों को लागू करते हैं
- स्थानीय बाज़ारों का प्रबंधन करना
- भूमि हस्तांतरण को रोकना
- अन्य चीजों के अलावा नशीले पदार्थों का विनियमन
- पहचान संरक्षण: ग्राम सभाओं के पास जनजातीय मामलों, सांस्कृतिक परंपराओं और पहचान के रखरखाव और गांव के आसपास के प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन पर अधिकार है।
- संघर्ष समाधान: इस प्रकार PESA अधिनियम ग्राम सभाओं को बाहरी या आंतरिक संघर्षों के खिलाफ अपने अधिकारों और परिवेश पर सुरक्षा जाल बनाए रखने में सक्षम बनाता है।
- सार्वजनिक निगरानी: ग्राम सभा को अपने गांवों की सीमाओं के भीतर नशीले पदार्थों के उत्पादन, वितरण, बिक्री और उपभोग को विनियमित करने और प्रतिबंधित करने का अधिकार होगा।
- गांधीवादी दर्शन: यह अधिनियम ग्राम स्वराज के गांधीवादी विचार पर आधारित है, जो संविधान के अनुच्छेद 40 (जो स्थानीय पंचायतों का आयोजन करता है) में सन्निहित है और PESA के पारित होने के साथ ही अस्तित्व में आया।
- पिछला अन्याय: इसके प्रावधानों ने यह आभास दिया कि एक उद्धारकर्ता प्रकट हुआ है, जो आदिवासी लोगों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को मिटा रहा है और उनके सम्मान और स्व-शासन के रीति-रिवाजों को बहाल कर रहा है।
पेसा अधिनियम, 1996 कैसे काम करता है?
- इसे अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- यह आदिवासी समुदायों, जो अनुसूचित क्षेत्रों के निवासी हैं, को स्वशासन की अपनी प्रणालियों के माध्यम से खुद पर शासन करने के अधिकार को मान्यता देता है, और प्राकृतिक संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को भी स्वीकार करता है।
- इस उद्देश्य के अनुसरण में, अधिनियम ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं को मंजूरी देने और सभी सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार देता है।
- इसमें वे प्रक्रियाएं और कर्मी शामिल हैं जो नीतियों को लागू करते हैं, छोटे (गैर-लकड़ी) वन संसाधनों, छोटे जल निकायों और छोटे खनिजों पर नियंत्रण रखते हैं, स्थानीय बाजारों का प्रबंधन करते हैं, भूमि हस्तांतरण को रोकते हैं और अन्य चीजों के बीच नशीले पदार्थों को विनियमित करते हैं।
- राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने संबंधित पंचायती राज अधिनियमों में बिना कोई कानून बनाए संशोधन करें जो PESA के जनादेश के साथ असंगत होगा।
- पेसा अधिनियम लागू होने के बाद, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने मॉडल पेसा नियम प्रसारित किए। अब तक छह राज्यों ने इन नियमों को अधिसूचित कर दिया है, जिनमें गुजरात भी शामिल है।
पेसा अधिनियम के परिणाम
अपनी स्थापना के बाद से, पेसा अधिनियम ने आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने और विकास प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:
- इस अधिनियम ने आदिवासी समुदायों को ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के माध्यम से विकास प्रक्रिया में अधिक भागीदारी देकर उनके सशक्तिकरण में योगदान दिया है।
- अधिनियम के अनुसार किसी भी भूमि के अधिग्रहण या हस्तांतरण से पहले ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है, जिससे बाहरी लोगों द्वारा आदिवासी समुदायों के शोषण को रोकने में मदद मिली है।
- इस अधिनियम ने आदिवासी समुदायों की परंपराओं और जीवन शैली की रक्षा के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाओं के संरक्षण में योगदान दिया है।
- इस अधिनियम ने ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को अधिक शक्तियाँ और कार्य देकर विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया है।
- इसने अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पेयजल जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुंच में सुधार में योगदान दिया है।
पेसा अधिनियम 1996 चुनौतियाँ
- देश के गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय समुदाय इस अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं और इसके प्रावधानों तक उनकी पहुंच नहीं है।
- अनुसूचित क्षेत्रों में कई आदिवासी समुदायों को पेसा अधिनियम के अधिकारों और अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है।
- ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के पास अक्सर अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं।
- कई ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों में अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की कमी है।
- राजनीतिक हस्तक्षेप: यह आवश्यक है कि ग्राम सभा से परामर्श किया जाए, लेकिन ग्राम सभा के निर्णयों का अक्सर सम्मान नहीं किया जाता है और वे राजनीतिक हस्तक्षेप के अधीन होते हैं।
- PESA अधिनियम कभी-कभी वन अधिकार अधिनियम और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जैसे अन्य कानूनों के साथ टकराव में पड़ सकता है, जो इसके कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
आगे बढ़ने का रास्ता
- अधिनियम का उल्लंघन और इसका कमजोर होना विकास के एक पैटर्न को उजागर करता है जो ग्राम सभाओं को मजबूत करने के प्रति केंद्र और राज्यों की प्रतिबद्धता की कमी को दर्शाता है।
- पेसा का अनुपालन करने के लिए राज्य सरकारों को अपने कानूनों में बदलाव करने की जरूरत है और भूमि अधिग्रहण, उत्पाद शुल्क, वन उपज, खानों और खनिजों, कृषि उपज बाजार और धन उधार से संबंधित कानूनों में संशोधन करने की जरूरत है।
- पेसा के बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आदिवासियों के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठनों को शामिल करने की आवश्यकता है क्योंकि वे जमीनी हकीकत और आदिवासी लोगों के सामने आने वाले मुद्दों से बेहतर वाकिफ हैं।
- पेसा अपनी भावना के अनुरूप एक अच्छा कानून है, लेकिन इसका कोई मतलब तभी होगा जब इसे गंभीरता से लिया जाए और अच्छी तरह से लागू किया जाए।
सरकार ने 1996 में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (PESA) अधिनियम लागू किया। निम्नलिखित में से कौन सा इसके उद्देश्य के रूप में पहचाना नहीं गया है?
(ए) स्वशासन प्रदान करना
(बी) पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना
(c) आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र बनाना
(d) आदिवासी लोगों को शोषण से मुक्त कराना
उत्तर: सी
अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम (पीईएसए), 1996 को आदिवासी लोगों की स्थानीय परंपराओं और सांस्कृतिक प्रथाओं के संरक्षण की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था। इस संदर्भ में पेसा अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करें और इसके कार्यान्वयन में क्या चुनौतियाँ हैं?